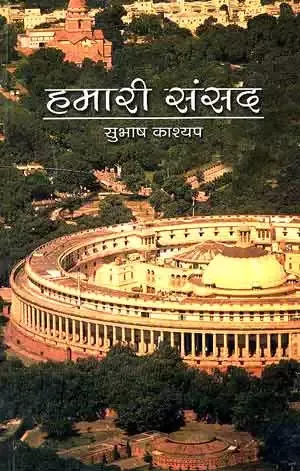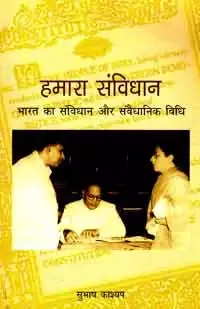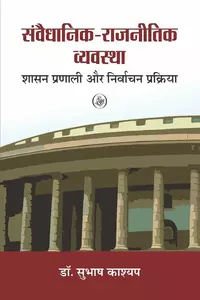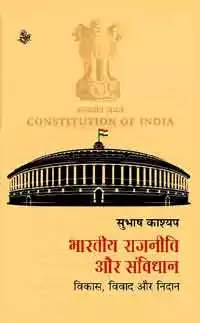|
इतिहास और राजनीति >> हमारी संसद हमारी संसदसुभाष काश्यप
|
372 पाठक हैं |
|||||||
भारत देश के दोनों सदनों का वर्णन
Hamari Sansad
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘‘इस पुस्तक में डॉ. कश्यप ने हमारे अपने सदनों में व्यवस्था रखने के लिए आवश्यक संसदीय प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण किया है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम लोग जानें कि उनके नाम पर प्रतिनिधी क्या काम करते हैं...
यह जरूरी है कि संसदीय प्रक्रियाओं को हम ऐसे शब्दों और मुहावरों में पेश करें कि जिन्हें आम जनता समझ सके। और, इस प्रशंसनीय पुस्तक में डॉ. कश्यप ने यही किया है। इन्होंने बहुत-सी उलझी प्रक्रियाओं को निखारकर सीधी-सादी भाषा में प्रस्तुत किया है...
मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक को भारी सफलता मिलेगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अधिक-से अधिक लोग इसे पढ़ें और भारत की जनता इसकी बहुत-बहुत प्रशंसा करे—भारत की जनता ही क्यों, सारी दुनिया के लोग ऐसा करें-क्योंकि डॉ. कश्यप संभवतया राष्ट्रमंडल के सबसे विशिष्ट संसदीय महासचिव हैं, वे सबसे वरिष्ठ महासचिवों में तो हैं ही। जब हम लोग अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाते हैं तो हम अनुभव करते हैं, न केवल राष्ट्रमंडल संसदीय सभाओं में अपितु अंतर्संसदीय संघ में इनकी प्रतिष्ठा कितनी ऊंची है।
अस्तु, डॉ. कश्यप, आपने बहुत बढ़िया काम किया। बधाई। मैं कामना करता हूँ कि इस पुस्तक को सारी सफलताएं मिलें !
यह जरूरी है कि संसदीय प्रक्रियाओं को हम ऐसे शब्दों और मुहावरों में पेश करें कि जिन्हें आम जनता समझ सके। और, इस प्रशंसनीय पुस्तक में डॉ. कश्यप ने यही किया है। इन्होंने बहुत-सी उलझी प्रक्रियाओं को निखारकर सीधी-सादी भाषा में प्रस्तुत किया है...
मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक को भारी सफलता मिलेगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अधिक-से अधिक लोग इसे पढ़ें और भारत की जनता इसकी बहुत-बहुत प्रशंसा करे—भारत की जनता ही क्यों, सारी दुनिया के लोग ऐसा करें-क्योंकि डॉ. कश्यप संभवतया राष्ट्रमंडल के सबसे विशिष्ट संसदीय महासचिव हैं, वे सबसे वरिष्ठ महासचिवों में तो हैं ही। जब हम लोग अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाते हैं तो हम अनुभव करते हैं, न केवल राष्ट्रमंडल संसदीय सभाओं में अपितु अंतर्संसदीय संघ में इनकी प्रतिष्ठा कितनी ऊंची है।
अस्तु, डॉ. कश्यप, आपने बहुत बढ़िया काम किया। बधाई। मैं कामना करता हूँ कि इस पुस्तक को सारी सफलताएं मिलें !
भूमिका
नेशनल बुक ट्रस्ट ने बड़ी सूझबूझ से वर्षों पूर्व फैसला किया कि एक ऐसी पुस्तक निकाली जाए जो आम लोगों के लिए भारतीय संसद की परिचायक हो। किसी-न-किसी कारण यह योजना अनेक हाथों से निकलती रही और यह कार्य संपन्न होने में बहुत उतार चढ़ाव आए। पुस्तक की पांडुलिपि तैयार होने में लगभग 10 वर्ष लग गए। नेशनल बुक ट्रस्ट का बहुत धन्यवाद कि 1991 में उन्होंने प्रथम हिंदी संस्करण को पाठकों के सामने रखा। यह और भी हर्ष का विषय है कि कुछ महीनों के अंदर ही उसकी सारी प्रतियां बिक गईं और पुनर्मुद्रण की आवश्यकता पड़ गई। 1993 में द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ और शीघ्र ही 1994 में उसका भी पुनर्मुद्रण हुआ। 1996 में तृतीय यथा संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ और एक के बाद छह आवृत्तियों की आवश्यकता पड़ी। प्रस्तुत चतुर्थ संस्करण में और भी ताजा सामग्री जोड़कर इसे अद्यतन बनाने का प्रयास किया गया है। भारतीय संसद की गत अर्द्धसदी की उपलब्धियों, सफलताओं-असफलताओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता एक समीक्षात्मक लेख भी जोड़ा गया है। आशा है पुस्तक की उपयोगिता बढ़ी होगी।
दुर्भाग्य की बात है। कि हमारी संसद के विषय में अभी तक कोई ऐसी पुस्तक उपलब्ध नहीं थी जो सरल एवं संक्षिप्त हो और जिसमें सभी जरूरी सामग्री भी दी गई हो। यह पुस्तक इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक प्रयास है। इसमें हमारी संसद के विषय में सुविधाजनक और सरल, गैर-तकनीकी, भाषा में कुछ आधारभूत तथ्य और प्रामाणिक तथा आज तक की ताजा जानकारी प्रस्तुत की गयी है। प्रत्येक स्थान पर इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि घटनाओं आदि का चित्रण निष्पक्ष और सरल हो। यह प्रयास किया गया है कि यथासंभव अनावश्यक ब्यौरे न दिए जाएं और विवादास्पद बातों में न पड़ा जाए। इस पुस्तक में संक्षेप में वर्णन किया गया है कि हमारी संसद वर्तमान रूप में कैसे आई, यह क्या है, इसके कृत्य क्या हैं, यह क्यों आवश्यक है, इसका गठन कैसे होता है और यह कैसे कार्य करती है। वस्तुतया इस पुस्तक का नाम ‘अपनी संसद को जानिए’ या ‘संसद-क्या, क्यों और कैसे’ भी हो सकता था।
प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह जानना आवश्यक है कि जिस देश का वह वासी है उसकी शासन व्यवस्था क्या है और उन संस्थाओं का स्वरूप क्या है जो उसके जीवन को शासित करती हैं और उसकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करती हैं। जैसा कि किसी ने कहा है, ‘‘इससे अधिक महत्व की बात कभी नहीं कही गई कि जो लोग अपनी सरकार के स्वरूप को नहीं समझते उनके लिए स्वतंत्रता और स्वतंत्र संस्थाओं को अधिक समय तक बनाए रखना संभव नहीं है’’। जो राजनीतिक प्रणाली हमने अपनाई है उसमें संसद लोगों की सर्वोच्च संस्था है और अपनी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता के प्रतीक के रूप में उनके लिए संसद को अच्छी तरह से जानना आवश्यक है।
इस पुस्तक के पहले ही अध्याय में वैदिक काल से प्रतिनिधि विधायी संस्थाओं के उद्भव और विकास का वर्णन करके यह प्रयास किया गया है कि संसद के अध्ययन को उचित ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखा जाए। इस बात की प्रायः उपेक्षा की जाती है कि आधुनिक काल में, विशेषकर भारत में, संसद कानून बनाने वाली संस्था, विधायी निकाय, होने के अतिरिक्त अन्य बहुत से कार्य भी करती है; सरकार पर राजनीतिक तथा वित्तीय नियंत्रण रखना, जनता का प्रतिनिधित्व करना और उसकी शिकायतें व्यक्त करना, संघर्षों का समाधान करना और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना इत्यादि इसके विभिन्न कृत्य हैं। इस पुस्तक में संसद के इन विविध क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है।
संसद का एक पहलू ऐसा है जिसका कि इस विषय पर लिखी गई अधिकांश पुस्तकों में सरसरी तौर पर ही उल्लेख किया गया है और वह है संसद के दोनों सदनों का वास्तविक कार्यकरण अर्थात्, उनकी बैठकें, पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, प्रश्नकाल और प्रस्ताव, बजट और विधायी प्रक्रिया इत्यादि। यह कहना आवश्यक नहीं कि हमारी राजनीतिक प्रणाली के सार्थक मूल्यांकन के लिए संसद के दोनों सदनों के वास्तविक कार्यकरण को अच्छी तरह समझना अनिवार्य है। अतः इन महत्त्वपूर्ण पहलुओं का पर्याप्त वर्णन करने का प्रयास किया गया है।
आधुनिक राज्य और प्रशासनिक कृत्यों का क्षेत्र इतना विशाल और जटिल है कि विधायी प्रस्तावों की पर्याप्त छानबीन करना और प्रशानिक कार्यों पर निगरानी रखना संसद के लिए असंभव हो जाता है। इसलिए लोकतंत्रात्मक जगत में लगभग सभी विधानमंडलों द्वारा संसदीय समिति प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय संसद ने भी अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए सहायता हेतु सुविकसित समिति प्रणाली अपनाई है। हमारी संसद में कार्य करने वाली विभिन्न समितियों, अर्थात् वित्तीय तथा सामान्य और स्थायी तथा तदर्थ समितियों का इस पुस्तक में विस्तृत विश्लेषण किया गया है। 17 नई विभागीय स्थायी समितियों का भी विवेचन किया गया है।
संसद का प्रभावपूर्ण होना काफी सीमा तक सचिवालय द्वारा इसे उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं पर निर्भर करता है। सचिवालय अपने दिन प्रति दिन के कार्य में कार्यपालिका से जितना स्वतंत्र होगा उतना ही निष्पक्ष और सही जानकारी वह उपलब्ध करा सकता है और ऐसी ही जानकारी के आधार पर सांसद अपने महत्त्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। स्वतंत्र सचिवालय का महत्व 1920 के शतक के बाद के वर्षों से ही महसूस किया जाने लगा था और इसलिए संसद के सदस्यों की सहायता करने वाली आदर्श संस्थाओं के रूप में लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय के विकास का भी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है।
संसदीय शिष्टाचार और संसदीय विशेषाधिकारों की प्रायः समाचारपत्रों आदि में चर्चा की जाती है। वस्तुतया हमारी विधायी संस्थाओं के गरिमापूर्ण एवं सार्थक कार्यकरण में ये मामले महत्व का स्थान रखते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों का अधिकांशतया गलत अर्थ लिया जाता है। वकीलों, पत्रकारों, सभी नागरिकों और स्वयं सांसदों को इनकी सीमा का स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। मैंने प्रयास किया है कि न्यायिक व्याख्याओं और संसद के दोनों सदनों के, इनकी समितियों के और पीठासीन अधिकारियों के फैसलों के प्रकाश में इस महत्त्वपूर्ण सिद्धांत की परिधियों का विश्लेषण किया जाए।
हमारी संसद भारत के सभी नागरिकों के लिए है। यह पुस्तक केवल विद्वानों, व्यवसायियों और विशेषज्ञों के लिए न होकर, साधारण पाठकों, वयस्क नवशिक्षितों के लिए है। आशा है यह अधिक से अधिक लोगों द्वारा बड़ी रुचि से पढ़ी जाएगी, वे इससे लाभान्वित होंगे और यह सभी लोगों को संसद का बेहतर ज्ञान कराते हुए उन्हें एक दूसरे के निकट लाने में सहायक होगी।
मैं नेशनल बुक ट्रस्ट और इसके प्राधिकारियों का आभारी हूं। उन्होंने बड़ी शीघ्रता से और उत्कृष्ट रूप से सस्ते दामों पर यह पुस्तक प्रकाशित की है। मुझे विशेष प्रसन्नता है कि कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी यह पुस्तक उपलब्ध हो गई है और आशा है कि शीघ्र ही सभी भारतीय भाषाओं में इसके संस्करण प्रकाशित हो जाएंगे।
दुर्भाग्य की बात है। कि हमारी संसद के विषय में अभी तक कोई ऐसी पुस्तक उपलब्ध नहीं थी जो सरल एवं संक्षिप्त हो और जिसमें सभी जरूरी सामग्री भी दी गई हो। यह पुस्तक इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक प्रयास है। इसमें हमारी संसद के विषय में सुविधाजनक और सरल, गैर-तकनीकी, भाषा में कुछ आधारभूत तथ्य और प्रामाणिक तथा आज तक की ताजा जानकारी प्रस्तुत की गयी है। प्रत्येक स्थान पर इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि घटनाओं आदि का चित्रण निष्पक्ष और सरल हो। यह प्रयास किया गया है कि यथासंभव अनावश्यक ब्यौरे न दिए जाएं और विवादास्पद बातों में न पड़ा जाए। इस पुस्तक में संक्षेप में वर्णन किया गया है कि हमारी संसद वर्तमान रूप में कैसे आई, यह क्या है, इसके कृत्य क्या हैं, यह क्यों आवश्यक है, इसका गठन कैसे होता है और यह कैसे कार्य करती है। वस्तुतया इस पुस्तक का नाम ‘अपनी संसद को जानिए’ या ‘संसद-क्या, क्यों और कैसे’ भी हो सकता था।
प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह जानना आवश्यक है कि जिस देश का वह वासी है उसकी शासन व्यवस्था क्या है और उन संस्थाओं का स्वरूप क्या है जो उसके जीवन को शासित करती हैं और उसकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करती हैं। जैसा कि किसी ने कहा है, ‘‘इससे अधिक महत्व की बात कभी नहीं कही गई कि जो लोग अपनी सरकार के स्वरूप को नहीं समझते उनके लिए स्वतंत्रता और स्वतंत्र संस्थाओं को अधिक समय तक बनाए रखना संभव नहीं है’’। जो राजनीतिक प्रणाली हमने अपनाई है उसमें संसद लोगों की सर्वोच्च संस्था है और अपनी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता के प्रतीक के रूप में उनके लिए संसद को अच्छी तरह से जानना आवश्यक है।
इस पुस्तक के पहले ही अध्याय में वैदिक काल से प्रतिनिधि विधायी संस्थाओं के उद्भव और विकास का वर्णन करके यह प्रयास किया गया है कि संसद के अध्ययन को उचित ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखा जाए। इस बात की प्रायः उपेक्षा की जाती है कि आधुनिक काल में, विशेषकर भारत में, संसद कानून बनाने वाली संस्था, विधायी निकाय, होने के अतिरिक्त अन्य बहुत से कार्य भी करती है; सरकार पर राजनीतिक तथा वित्तीय नियंत्रण रखना, जनता का प्रतिनिधित्व करना और उसकी शिकायतें व्यक्त करना, संघर्षों का समाधान करना और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना इत्यादि इसके विभिन्न कृत्य हैं। इस पुस्तक में संसद के इन विविध क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है।
संसद का एक पहलू ऐसा है जिसका कि इस विषय पर लिखी गई अधिकांश पुस्तकों में सरसरी तौर पर ही उल्लेख किया गया है और वह है संसद के दोनों सदनों का वास्तविक कार्यकरण अर्थात्, उनकी बैठकें, पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, प्रश्नकाल और प्रस्ताव, बजट और विधायी प्रक्रिया इत्यादि। यह कहना आवश्यक नहीं कि हमारी राजनीतिक प्रणाली के सार्थक मूल्यांकन के लिए संसद के दोनों सदनों के वास्तविक कार्यकरण को अच्छी तरह समझना अनिवार्य है। अतः इन महत्त्वपूर्ण पहलुओं का पर्याप्त वर्णन करने का प्रयास किया गया है।
आधुनिक राज्य और प्रशासनिक कृत्यों का क्षेत्र इतना विशाल और जटिल है कि विधायी प्रस्तावों की पर्याप्त छानबीन करना और प्रशानिक कार्यों पर निगरानी रखना संसद के लिए असंभव हो जाता है। इसलिए लोकतंत्रात्मक जगत में लगभग सभी विधानमंडलों द्वारा संसदीय समिति प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय संसद ने भी अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए सहायता हेतु सुविकसित समिति प्रणाली अपनाई है। हमारी संसद में कार्य करने वाली विभिन्न समितियों, अर्थात् वित्तीय तथा सामान्य और स्थायी तथा तदर्थ समितियों का इस पुस्तक में विस्तृत विश्लेषण किया गया है। 17 नई विभागीय स्थायी समितियों का भी विवेचन किया गया है।
संसद का प्रभावपूर्ण होना काफी सीमा तक सचिवालय द्वारा इसे उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं पर निर्भर करता है। सचिवालय अपने दिन प्रति दिन के कार्य में कार्यपालिका से जितना स्वतंत्र होगा उतना ही निष्पक्ष और सही जानकारी वह उपलब्ध करा सकता है और ऐसी ही जानकारी के आधार पर सांसद अपने महत्त्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। स्वतंत्र सचिवालय का महत्व 1920 के शतक के बाद के वर्षों से ही महसूस किया जाने लगा था और इसलिए संसद के सदस्यों की सहायता करने वाली आदर्श संस्थाओं के रूप में लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय के विकास का भी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है।
संसदीय शिष्टाचार और संसदीय विशेषाधिकारों की प्रायः समाचारपत्रों आदि में चर्चा की जाती है। वस्तुतया हमारी विधायी संस्थाओं के गरिमापूर्ण एवं सार्थक कार्यकरण में ये मामले महत्व का स्थान रखते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों का अधिकांशतया गलत अर्थ लिया जाता है। वकीलों, पत्रकारों, सभी नागरिकों और स्वयं सांसदों को इनकी सीमा का स्पष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। मैंने प्रयास किया है कि न्यायिक व्याख्याओं और संसद के दोनों सदनों के, इनकी समितियों के और पीठासीन अधिकारियों के फैसलों के प्रकाश में इस महत्त्वपूर्ण सिद्धांत की परिधियों का विश्लेषण किया जाए।
हमारी संसद भारत के सभी नागरिकों के लिए है। यह पुस्तक केवल विद्वानों, व्यवसायियों और विशेषज्ञों के लिए न होकर, साधारण पाठकों, वयस्क नवशिक्षितों के लिए है। आशा है यह अधिक से अधिक लोगों द्वारा बड़ी रुचि से पढ़ी जाएगी, वे इससे लाभान्वित होंगे और यह सभी लोगों को संसद का बेहतर ज्ञान कराते हुए उन्हें एक दूसरे के निकट लाने में सहायक होगी।
मैं नेशनल बुक ट्रस्ट और इसके प्राधिकारियों का आभारी हूं। उन्होंने बड़ी शीघ्रता से और उत्कृष्ट रूप से सस्ते दामों पर यह पुस्तक प्रकाशित की है। मुझे विशेष प्रसन्नता है कि कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी यह पुस्तक उपलब्ध हो गई है और आशा है कि शीघ्र ही सभी भारतीय भाषाओं में इसके संस्करण प्रकाशित हो जाएंगे।
सुभाष काश्यप
1
संसदीय शासन प्रणाली का उद्भव एवं विकास
‘‘हमने संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली को सोच-समझकर ही चुना है; हमने इसे केवल इसी कारण नहीं चुना कि हमारा सोचने का तरीका कुछ हद तक ऐसा ही रहा बल्कि इस कारण भी कि यह प्रणाली हमारी पुरातन परंपराओं के अनुकूल है। स्वाभाविक है कि पुरातन परंपराओं का पुरातन स्वरूप में नहीं अपितु नई परिस्थितियों और नए वातावरण के अनुसार बदलकर अनुसरण किया गया है; इस पद्धति को चुनने का एक कारण यह भी है कि हमने देखा कि अन्य देशों में, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम में यह प्रणाली सफल रही है।’’
जवाहरलाल नेहरू
प्राचीन भारत में प्रतिनिधि निकाय
26 जनवरी, 1950 के दिन भारत नए गणराज्य के संविधान का शुभारंभ हुआ और भारत अपने लंबे इतिहास में पहली बार एक आधुनिक संस्थागत ढांचे के साथ पूर्व संसदीय लोकतंत्र बना। लोकतंत्र एवं प्रतिनिधि संस्थाएं भारत के लिए पूर्णतया नई नहीं हैं। कुछ प्रतिनिधि निकाय तथा लोकतंत्रात्मक स्वशासी संस्थाएं वैदिक काल में भी विद्यमान थीं (सिरका 3000-1000 ईसा पूर्व)। ऋग्वेद में ‘सभा’ तथा ‘समिति’ नामक दो संस्थाओं का उल्लेख है। वहीं से आधुनिक संसद की शुरुआत मानी जा सकती है। इन दो संस्थाओं का दर्जा और इनके कृत्य अलग-अलग थे। ‘समिति’ एक आम सभा या लोक सभा हुआ करती थी और ‘सभा’ अपेक्षतया छोटा और चयनित वरिष्ठ लोगों का निकाय, जो मोटे तौर पर आधुनिक विधानमंडलों में उपरि सदन के समान था।
वैदिक ग्रंथों में ऐसे अनेक संकेत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि ये दो निकाय राज्य के कार्यों से निकट का संबंध रखते थे और इन्हें पर्याप्त प्राधिकार, प्रभुत्व एवं सम्मान प्राप्त था। ऐसा ज्ञात होता है कि आधुनिक संसदीय लोकमत के कुछ महत्त्वपूर्ण तत्व, जैसे निर्बाध चर्चा और बहुमत द्वारा निर्णय, तब भी विद्यमान थे। बहुमत से हुआ निर्णय ‘‘अलंघनीय माना जाता था जिसकी अवहेलना नहीं हो सकती थी क्योंकि जब एक सभा में अनेक लोग मिलते हैं और वहां एक आवाज से बोलते हैं, तो उस आवाज या बहुमत की अन्य लोगों द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती।’’ वास्तव में प्राचीन भारतीय समाज का मूल सिद्धांत यह था कि शासन का कार्य किसी एक व्यक्ति की इच्छानुसार नहीं बल्कि पार्षदों की सहायता से संयुक्त रूप से होना चाहिए। पार्षदों का परामर्श आदर से माना जाता था।
वैदिक काल के राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार ‘धर्म’ को वास्तव में प्रभुत्व दिया जाता था और ‘धर्म’ अथवा विधि द्वारा शासन के सिद्घांत को राजा द्वारा माना जाता था और लागू किया जाता था। आदर्श यह था कि राजा की शक्तियां जनेच्छा और रीति-रिवाजों, प्रथाओं, और धर्मशास्त्रों के आदेशों द्वारा सीमित होती थीं। राजा को विधि तथा अपने क्षेत्र के विधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी और अपनी जनता के भौतिक तथा नैतिक कल्याण के लिए राज्य को न्यास अथवा ट्रस्ट के रूप में रखना होता था। यद्यपि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतया राजतंत्रवादी हुआ करती थी, फिर भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां राजा का चुनाव होता था। जो भी हो, कुछ लोकतंत्रात्मक संस्थाएं एवं प्रथाएं प्रायः हमारी राजतंत्रीय शासन प्रणाली का सदा अभिन्न अंग रहीं।
वैदिक ग्रंथों में ऐसे अनेक संकेत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि ये दो निकाय राज्य के कार्यों से निकट का संबंध रखते थे और इन्हें पर्याप्त प्राधिकार, प्रभुत्व एवं सम्मान प्राप्त था। ऐसा ज्ञात होता है कि आधुनिक संसदीय लोकमत के कुछ महत्त्वपूर्ण तत्व, जैसे निर्बाध चर्चा और बहुमत द्वारा निर्णय, तब भी विद्यमान थे। बहुमत से हुआ निर्णय ‘‘अलंघनीय माना जाता था जिसकी अवहेलना नहीं हो सकती थी क्योंकि जब एक सभा में अनेक लोग मिलते हैं और वहां एक आवाज से बोलते हैं, तो उस आवाज या बहुमत की अन्य लोगों द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती।’’ वास्तव में प्राचीन भारतीय समाज का मूल सिद्धांत यह था कि शासन का कार्य किसी एक व्यक्ति की इच्छानुसार नहीं बल्कि पार्षदों की सहायता से संयुक्त रूप से होना चाहिए। पार्षदों का परामर्श आदर से माना जाता था।
वैदिक काल के राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार ‘धर्म’ को वास्तव में प्रभुत्व दिया जाता था और ‘धर्म’ अथवा विधि द्वारा शासन के सिद्घांत को राजा द्वारा माना जाता था और लागू किया जाता था। आदर्श यह था कि राजा की शक्तियां जनेच्छा और रीति-रिवाजों, प्रथाओं, और धर्मशास्त्रों के आदेशों द्वारा सीमित होती थीं। राजा को विधि तथा अपने क्षेत्र के विधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी और अपनी जनता के भौतिक तथा नैतिक कल्याण के लिए राज्य को न्यास अथवा ट्रस्ट के रूप में रखना होता था। यद्यपि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतया राजतंत्रवादी हुआ करती थी, फिर भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां राजा का चुनाव होता था। जो भी हो, कुछ लोकतंत्रात्मक संस्थाएं एवं प्रथाएं प्रायः हमारी राजतंत्रीय शासन प्रणाली का सदा अभिन्न अंग रहीं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book